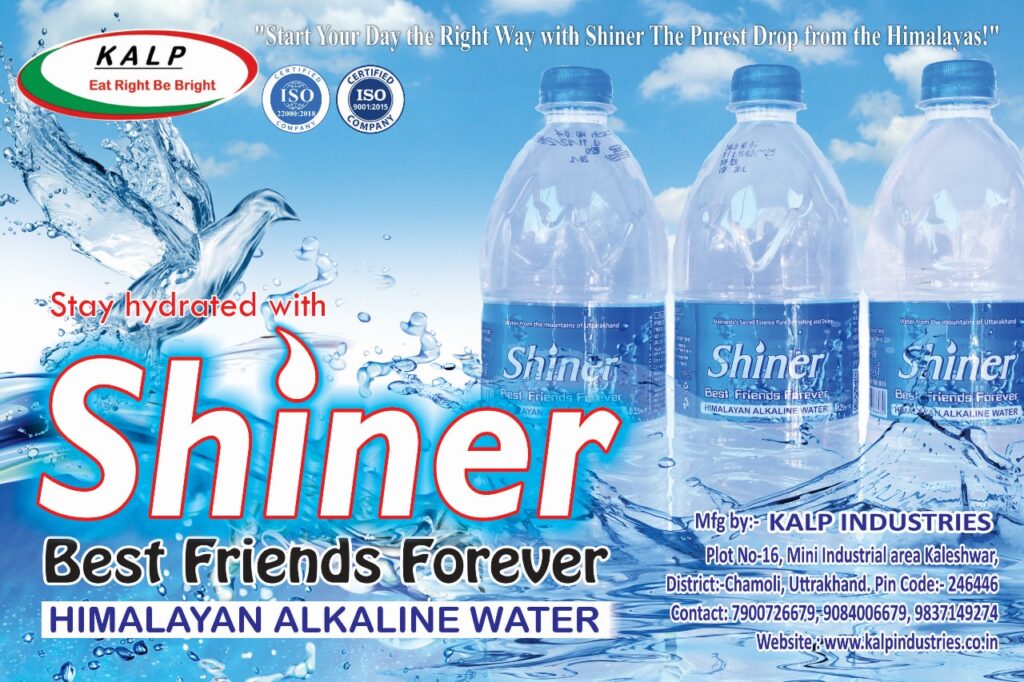लोक संस्कृति से विलुप्त होती ढोल विधा


मणि भारती
मध्य हिमालय गढ़वाल और कुमाऊं हमारी पर्वतीय संस्कृति के लोक मानस की सामाजिक सम्पन्नता का आधर है। पहाड़ की लोकमाटी की संस्कृति के सम्वाहक हमारे पारम्परिक वाद्य हैं, जो आदिकाल से चले आ रहे हैं। इन वाद्यों में प्रमुख वाद्य ‘ढोल’ है। इसका सहायक वाद्य दमाऊं ;दमागाद्ध है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। ढोल पहाड़ की लोक संस्कृति का एक अभिव्यक्त रूप है। इसका अध्यात्मिक महत्व है। ढोल को सृष्टि का प्राचीन अध्यात्मिक वाद्य कहा गया है। जिसका उल्लेख वेदों, पुराणों और रामायण में मिलता है। सर्वप्रथम ढोल को भगवान शिव ने ही धरण किया। संसार के सृजन का क्रम ढोल नाद से हुआ। जिस प्रकार सर्वप्रथम वेद-ब्रहमा जी के मुख से निकले, उनका विध्वित आलेखन और विभाजन कर कर उन्हें चार वेदों का स्वरूप वेद व्यास जी द्वारा दिया गया। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने सृष्टि के संहार के पश्चात सृजन की निष्बध्ता को विनिष्ठ करने के लिए की थी।
जिस समय भगवान शंकर और महाशक्ति देवी पार्वती के बीच ढोल सम्बन्ध्ति संवाद चल रहा था उस समय वहाँ श्रोता के रूप में एक ‘औजि’ एक जाति विशेष का व्यक्ति भी था जिसने ढोल सम्बन्ध् िसंवाद-वृतांत को ध्यान से सुना और कंठस्थ किया और इस ढोल विध की परम्परा को पारंगत बाजीगरों ने मौखिक रूप से पीड़ी दर पीड़ी आगे बढ़ाया। पहाड़ों में प्रायः शुभ, मांगलिक कार्यों, धर्मिक अनुष्ठानों, मंडाणों, उत्सवों और पहाड़ी मेलों में शगुन तथा मंगल की कामना करने तथा अमंगल को हरने वाला कहा गया है। इसी लिए ढोल का अध्यात्मिक महत्व भी है। ढोल सागर का संग्रह सन् 1913 में स्वर्गीय राय साहब पं. ईश्वरी दत्त घिल्डियाल जी, तहसीलदार साहब ;आलेखों द्वारा साभारद्ध के प्रयत्नों से संभव हो सका। पं. ईश्वरी दत्त जी ढोल विद्या में पारंगत थे। उनके सहयोगी स्व. पंडित गिरिजा दत्त नैथानी तथा भोला दत्त जी काला के सहयोग से पं. ब्रहमा नन्द जी थपलियाल ने बद्रीकेदार प्रेस पौड़ी से प्रकाशित किया। शनै-शनै लोक संस्कृति के विद्वानों अबोध् बन्धु बहुगुणा जी और मोहन लाल बाबुलकर जी ने समय-समय पर विभिन्न पत्रा-पत्रिकाओं में ढोल विध पर लेख प्रकाशित कर जिज्ञासू पाठकों तक इस कला को पहुंचाया। इसी क्रम में डा0 शिवानन्द नौटियाल जी ने भी अपनी किताब ‘गढ़वाल के लोकगीत’ में स्व. पं. केशव अनुरागी द्वारा संग्रहित एवं उनका प्रयोगात्मक अध्ययन प्रकाशित किया और कुछ समय बाद यह ‘नाद-नन्दनी’ नामक ग्रंथ प्रकाशित किया गया जो कि आज बाजार में उपलब्ध् है। इस पुस्तक में स्व. अनुरागी जी का बहुत बड़ा योगदान है। स्व. अनुरागी जी की मृत्यु के पश्चात् ढोल सागर का अधूरा कार्य स्व. डा0 शिवानन्द नौटियाल जी ने पूर्ण किया। किन्तु इस विध का पूर्ण स्वरूप व विधन पूर्ण नहीं है। आज अनेकों विद्वान, संस्कृत कर्मी इस विध पर शोध् कार्य कर रहे हैं। ढोल को ईश्वर पुत्रा भी कहा गया है।
ढोल की बनावट और धतु-
ढोल तांबे की धतु का बना होता है, जिसके विभिन्न अंग कंदोटी ;स्कन्द पट्टिकाद्ध, चाक, ;पट्टिका में लगा कुण्डलद्ध, पूड़ विजैसार ;पीतल की पट्टिकाद्ध, कुंडली, कसणी डोरी, लाकुड़ ;बजाने की लकड़ीद्ध आदि।


ढोल सागर में इनका विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके जो अंग-प्रत्यंग हैं वे किसी न किसी के पुत्रा हैं। यहाँ तक कि इससे निकलने वाला नाद ;स्वरद्ध भी वायु पुत्रा है। यदि वायुमंडल न हो तो नाद कैसे गूंजेगा? ढोल को अध्यात्मिक व दैवीय स्वरूप देने के लिए ढोल सागर के रचियता ने इसकी डोरियों को ब्रहमा का पुत्रा तो बजाने वाली डंडियों को भीम पुत्रा, चमेड़ के पूड़ को विष्णु पुत्रा कहा। कुण्डलों को नाग पुत्रा तो कांधे पर डालने वाले कंदोलियों को कुर्म पुत्रा और कणिंकाओं को गुणियों से उत्पन्न बताया गया है। ढोल का सहायक वाद्य दमाउफॅ ;दमामाद्ध है जो ढोल के साथ आवश्यक रूप से बजाया जाता है। दमामा भी तांबे की धतु का बना होता है। इसकी आकृति अधर््गोलाकार गहरी कढ़ाही जैसी होती है। दमाउफॅं जमीन में रखकर दो लकड़ीयों से बजाया जाता है या गले में लटकाकर चलते-चलते बजाया जाता है। ढोल सागर नाद का शास्त्राीय ग्रन्थ है जिसमें ढोल बजाने के नियम तथा पद्वतियों का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। ढोल विद्या की चार प्रमुख शैलियां हैं जो क्रमशः बढै, धुयेल, शबद और रहमानी। इनका सबका अपना महत्व है।
बढै ;बधईद्ध- यह शुभ मांगलिक अवसरों जैसे पुत्रा का जन्म, गृह प्रवेश और विवाह के अवसर पर शुभकामना, बधई के रूप में बजाई जाती है।
धुयेल – प्रातः एवं संध्या के समय गांव के मन्दिरों, देवालयों में देव पूजन के लिए बजाया जाता है।
शबद – इसे बजाने में उत्थान, अवरोध्, उत्तेजन और विश्रान्ति के सघन रूप को प्रकट करता है। शक्ति को जगाने व बारात के आने की सूचना देने के लिए होता है।
नौबत – पुराने काल में राज दरबार में बजाने की परम्परा रही है। प्रायः रात्राी के अन्तिम प्रहर में मंगल कार्यों में बजाया जाता था।
रहमानी – यह ताल चलते-चलते ढोल बजाने की कला का नाम है। प्रायः इसे वर यात्रा ;बारातद्ध में बजाया जाता है।
स्व. केशव अनुरागी जी ने ढोल की इन तालों का लिपिब( स्पष्टीकरण इस प्रकार से किया-
बढै ;बधईद्ध- झेगु झोग्गा { झोग्गा { तोझे गा{ता{ झेगु नझे ग ता ग झे गा।
ध्ुँयेल – झेगु झेगु झेगु तग तु।
शबद – झेगु झेगु झेनन् झेनन् तू झेन।
रहमानी – झेगु तक झेगु तक। झेग न झेगतु। झे{ नन तक।
आज इस विध पर हम जितना भी अध्ययन करें या लिखें शायद कम होगा। एक बात तो सत्य है कि किसी समय हमारे समाज में ढोल विध के बाजीगरों का एक विशेष स्थान था। कोई भी मांगलिक कार्य इनके बिना अध्ूरा रहता था। जिनको इस विध पर पारंगता हासिल थी उनका बड़ा आदर और सम्मान हुआ करता था।
देवी-देवताओं को अपनी इस विध द्वारा आह्वान कर प्रकट करने की क्षमता रखते थे। मण्डाण या कोई भी शुभ मांगलिक कार्यों में इनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। किन्तु दुर्भाग्य कि बात है कि आज ये लोग अपने ही समाज में उपेक्षा के पात्रा हैं। इसका मूल कारण है पहाड़ों से पलायन। अपनी मूल संस्कृति को भूल पाश्चात्य संस्कृति की ओर झुकाव, उसके प्रति आकर्षण। जिसके चलते हमारी प्राचीन विध विलुप्ति के कगार पर आ खड़ी हुई है। जो एक चिंता एवं सोचनीय विषय है। आज हमें अपने पारम्परिक मूल संस्कृति को संजोने के लिए आगे आना ही होगा और अपनी सांस्कृतिक ध्रोहरों को समृ( बनाये रखने एवं संरक्षण हेतु गम्भीरता से विचार करना होगा।
आज लोक संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें अनेकों योजनायें चला रही हैं। जिसका लाभ सब कलाकारों को नहीं मिल पाता। इसका मूल कारण है पहाड़ों से पलायन, जिस कारण पहाड़वासी अपनी मूल संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इस विषय में सरकार दूर-सुदूर पहाड़ों में बसे बाजीगर जो इस विध को अपने में ही संजोये बैठे हैं और उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं उनको खोज निकालना पड़ेगा और उनकी इस अमूल्य ध्रोहर को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उन्हें आमंत्रित कर उनका सम्मान करना होगा। पहाड़ों पर स्थान-स्थान पर कुछ खास अवसरों पर ‘ढोल विध’ की कार्यशालाओं का आयोजन हेतु उनकी सेवा लेनी चाहिए और उनको मार्ग व्यय, रहने का खर्च व मानदेय देकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए।
लेखक आकाशवाणी व दूरदर्शन के लोक कलाकार हैं.